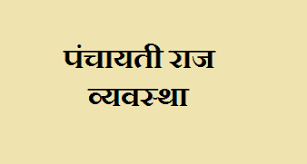गुरु रविदास जी की जीवन यात्रा में दिखता है ज्ञान भक्ति का अदभुद संगम।
गुरु रविदास जी को कर्म के प्रति महान कार्यों के लिए जाना जाता है। उनके समय में दलित लोगों को बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था और उन्हें समाज में अन्य जाति के लोगों से दूर रखा जाता था। उन्हें किसी भी मंदिर में प्रभु पूजा करने के लिए नहीं जाने दिया जाता था और दलित बच्चों के साथ स्कूलों आदि में भी भेद भाव किया जाता था। ऐसे समय में गुरु रविदास जी ने दलित समाज के लोगों को एक नया अध्यात्मिक सन्देश दिया जिससे की वो इस तरीके की मुश्किलों का डटकर सामना कर सकें।

प्रभु जी, तुम मोती, हम धागा जैसे सोनहिं मिलत सोहागा॥
भारत एक ऐसा देश है जिसकी मिटटी में समय समय पर साधू संतो ने अवतार लेकर पृथ्वीवासियों को ईश्वर-भक्ति,सत्य व् ज्ञान से परिचित करवाया है। गुरु रविदास भी ऐसे महान संतों में अग्रणी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत में स्थापित ब्राह्मणी व्यवस्था और खंडवाद अंडम्बरवाद अंध विश्वास को खत्म करने में बहुत अहम भूमिका निभायी। इनकी लोकवाणी युक्त रचनाओं ने जनमानस पर ऐसा अमिट प्रभाव डाला कि आज के भारत में भी लोग इन्हे बड़े आदर भाव से याद करते है।
वैसे तो महान संत गुरु रविदास के जन्म से जुडी जानकारी बहुत कम मिलती है लेकिन फिर भी हम इतिहास के पन्नों से मिली जानकारी के आधार पर ये कह सकते है कि महान संत गुरु रविदास का जन्म लगभग सन 1433 ईस्वी के आसपास हुआ है। इनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है “चौदह से तैंतीस कि माघ सुदी पन्दरास”
हिन्दू धर्म महीने के अनुसार महान संत गुरु रविदास का जन्म माघ महीने के पूर्णिमा के दिन माना जाता है और इसी दिन हमारे देश में महान संत गुरु रविदास की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। संत रविदास का जन्म सन् 1388 (इनका जन्म कुछ विद्वान 1398 में हुआ भी बताते हैं) को बनारस में हुआ था। इनको संत कबीर का समकालीन माना गया है। संत कबीर की तरह गुरु रैदास भी संत कोटि के प्रमुख कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। कबीर ने ‘संतन में रविदास’ कहकर इन्हें बहुत बड़ी मान्यता दी है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा : दुखियों का दुःख हरने आये गुरु रविदास जी के पिता का नाम राहू तथा माता का नाम करमा था। इन्हे बचपन से ही साधु-सन्तों की संगति से पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की ललक थी। कहा जाता है कि बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदा नंद के पाठशाला गये जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा वहाँ दाखिला लेने से रोका किया गया था। हालाँकि पंडित शारदा ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक न होकर एक ईश्वर के द्वारा भेजी गयी संतान है।
अत: पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया और उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। रविदास बचपन से ही बहुत ही तेज और होनहार थे। इसलिए गुरु पंडित शारदा नंद उनसे बहुत प्रभावित रहते थे उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रुप से प्रबुद्ध और बड़े महान सामाजिक सुधारक के रुप में जाने जायेंगे।
रैदास जी का स्वभाव : जानकारों से पता चलता है कि वे वचन पालन सम्बन्धी गुणों के धनि थे। कहा जाता है कि एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा-स्नान के लिए जा रहे थे। गुरु रविदास जी के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा-स्नान के लिए मैं अवश्य चलता किन्तु । गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा ? मन जो काम करने के लिए अन्त:करण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इसे कठौते के जल में ही गंगास्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गयी कि –
“मन चंगा तो कठौती में गंगा”
गुरु रविदास जी का विशवास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित-भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। उन्होंने अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता के साथ साथ शिष्टता के गुणों का विकास करने पर बहुत ज़ोर दिया। अपने एक पद में उन्होंने लिखा है कि
“कह रैदास तेरी भगति दूरि है, भाग बड़े सो पावै। तजि अभिमान मेटि आपा पर, पिपिलक हवै चुनि खावै।”

उनके ऐसे ही पदों में उनकी वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना के साथ साथ मानव प्रेम की भावना सरल रूप से देखी जा सकती है। उनके सत्संगों, भजनो और उपदेशों से ऐसी शिक्षा मिलती है कि हर कोई बहुत ही सरलता से उनका अनुयायी बन जाता है।
समाज के सभी वर्गों उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि लोग उनके प्रति भक्त बन गये। इतिहास के पन्ने बताते है कि मीराबाई उनकी भक्ति-भावना से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने रैदास जी को अपने गुरु के रूप स्वीकारा और अपने इष्ट कृष्ण को पाया। मीराबाई का मानना था कि उन्हे प्रभु कृष्ण से मिलाने वाले केवल गुरु रैदास ही थे।
वर्णाश्रम अभिमान तजि, पद रज बंदहिजासु की। सन्देह-ग्रन्थि खण्डन-निपन, बानि विमुल रैदास की।।
रविदासजी का वैवाहिक जीवन : कहा जाता है कि प्रभु के प्रति उनका घनिष्ट प्रेम और भक्ति के कारण वो अपने पारिवारिक व्यापार और माता-पिता से लगातार दूर हो रहे थे। यह देख कर उनके माता-पिता ने उनका विवाह “श्रीमती लोना देवी” से करवा दिया और उनसे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम “विजय दास” था। विवाह के बाद भी वो अपने परिवार के व्यापार में सही तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रहे थे।
जाति-जाति में जाति हैं, जो केतन के पात।
रैदास मनुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात।।
यह देखते हुए उनके बेटे ने एक दिन उन्हें घर से ये देखने के लिए निकल दिया कि वे परिवार की मदद के बिना कैसे अपने सामजिक कार्यों को कर सकते है। लेकिन इस घटना के बाद रैदास जी घर के पीछे रहने लगे और अपने सामजिक कार्यों पूरी तरह से जुट गये। बाद में गुरु रविदास जी राम रूप के भक्त बन गए और राम, रघुनाथ, रजा राम चन्द्र, कृष्णा, हरी, गोविन्द के नामों का उच्चारण करके प्रभु के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने लगे।
मन ही पूजा मन ही धूप ,मन ही सेऊँ सहज सरूप।
सामाजिक मुद्दे और रविदास :वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव-विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रन्थों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है।

“कृस्न, करीम, राम, हरि, राघव, जब लग एक न पेखा। वेद कतेब कुरान, पुरानन, सहज एक नहिं देखा।।
चारो वेद के करे खंडौती । जन रैदास करे दंडौती”।
गुरु रविदास जी को कर्म के प्रति महान कार्यों के लिए जाना जाता है। उनके समय में दलित लोगों को बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था और उन्हें समाज में अन्य जाति के लोगों से दूर रखा जाता था। उन्हें किसी भी मंदिर में प्रभु पूजा करने के लिए नहीं जाने दिया जाता था और दलित बच्चों के साथ स्कूलों आदि में भी भेद भाव किया जाता था। ऐसे समय में गुरु रविदास जी ने दलित समाज के लोगों को एक नया अध्यात्मिक सन्देश दिया जिससे की वो इस तरीके की मुश्किलों का डटकर सामना कर सकें।
अपने गुणों के कारण सन्त रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं।
रैदास के 40 पद गुरु ग्रन्थ साहब में मिलते हैं जिसका सम्पादन गुरु अर्जुन सिंह देव ने 14 वीं सदी में किया था । उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं।