भारतीय मीडियाः गरिमा बहाली की चुनौती-प्रो. संजय
पत्रकार की पोलिटकल लाइन तो हो किंतु उसकी पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए।
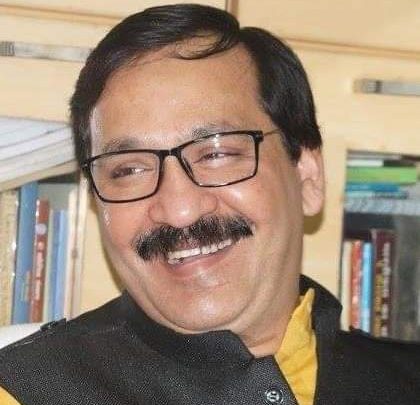
भारतीय मीडिया का यह सबसे त्रासद समय है। छीजते भरोसे के बीच उम्मीद की लौ फिर भी टिमटिमा रही है। उम्मीद है कि भारतीय मीडिया आजादी के आंदोलन में छिपी अपनी गर्भनाल से एक बार फिर वह रिश्ता जोड़ेगा और उन आवाजों का उत्तर बनेगा जो उसे कभी पेस्टीट्यूट, कभी पेड न्यूज तो कभी गोदी मीडिया के नाम पर लांछित करती हैं। जिनकी समाज में कोई क्रेडिट नहीं वह आज मीडिया का हिसाब मांग रहे हैं। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे लोग, वाणी और कृति से अविश्वास के प्रतीक भी मीडिया से शुचिता की मांग कर रहे हैं।
देखा जाए तो यह गलत भी नहीं है। मेरे गलत होने से आपको गलत होने की आजादी नहीं मिल जाती। एक पाठक और एक दर्शक के नाते हमें तो श्रेष्ठ ही चाहिए, मिलावट नहीं। वह मिलावट खबरों की हो या विचारों की। लेकिन आज के दौर में ऐसी परिशुद्धता की अपेक्षा क्या उचित है? क्या बदले हुए समय में मिलावट को युगधर्म नहीं मान लेना चाहिए? आखिर मीडिया के सामने रास्ता क्या है? किन उपायों और रास्तों से वह अपनी शुचिता, पवित्रता, विश्वसनीयता और प्रामणिकता को कायम रख सकता है, यह सवाल आज सबको मथ रहा है। जो मीडिया के भीतर हैं उन्हें भी, जो बाहर हैं उन्हें भी।

खबरों में मिलावट का समयः सबसे बड़ी चुनौती खबरों में मिलावट की है। खबरें परिशुद्धता के साथ कैसे प्रस्तुत हों, कैसे लिखी जाएं, बिना झुकाव, बिना आग्रह कैसे वे सत्य को अपने पाठकों तक संप्रेषित करें। क्या विचारधारा रखते हुए एक पत्रकार इस तरह की साफ-सुथरी खबरें लिख सकता है? ऐसे सवाल हमारे सामने हैं। इसके उत्तर भी साफ हैं, जी हां हो सकता है। हमारे समय के महत्त्वपूर्ण पत्रकार और संपादक श्री प्रभाष जोशी हमें बताकर गए हैं। वे कहते थे
“पत्रकार की पोलिटकल लाइन तो हो किंतु उसकी पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए।”
प्रभाष जी का मंत्र सबसे प्रभावकारी है, अचूक है। सवाल यह भी है कि एक विचारवान पत्रकार और संपादक विचार निरपेक्ष कैसे हो सकता है? संभव हो उसके पास विचारधारा हो, मूल्य हों और गहरी सैंद्धांतिकता का उसके जीवन और मन पर असर हो। ऐसे में खबरें लिखता हुआ वह अपने वैचारिक आग्रहों से कैसे बचेगा ? अगर नहीं बचेगा तो मीडिया की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का क्या होगा? उत्पादन के कारखानों में ‘क्वालिटी कंट्रोल’ के विभाग होते हैं। मीडिया में यह काम संपादक और रिर्पोटर के अलावा कौन करेगा? तथ्य और सत्य का संघर्ष भी यहां सामने आता है। कई बार तथ्य गढ़ने की सुविधा होती है और सत्य किनारे पड़ा रह जाता है। पत्रकार ऐसा करते हुए खबरों में मिलावट कर सकता है। वह सुविधा से तथ्यों को चुन सकता है, सुविधा से परोस सकता है। इन सबके बीच भी खबरों को प्रस्तुत करने के आधार बताए गए हैं, वे अकादमिक भी हैं और सैद्धांतिक भी। हम खबर देते हुए न्यायपूर्ण हो सकते हैं। ईमान की बात कर सकते हैं। परीक्षण की अनेक कसौटियां हैं। उस पर कसकर खबरें की जाती रही हैं और की जाती रहेंगी। विचारधारा के साथ गहरी लोकतांत्रिकता भी जरुरी है जिसमें आप असहमति और अकेली आवाजों को भी जगह देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। एजेंडा पत्रकारिता के समय में यह कठिन जरूर लगता है पर मुश्किल नहीं।
बौद्धिक विमर्शों से टूटता रिश्ताः हिंदी पत्रकारिता पर आरोप लग रहे हैं कि वह अपने समय के सवालों से कट रही है। उन पर बौद्धिक विमर्श छेड़ना तो दूर, वह उन मुद्दों की वास्तविक तस्वीर सूचनात्मक ढंग से भी रखने में विफल पा रही है तो यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्यों है। 1990 के बाद के उदारीकरण के सालों में अखबारों का सुदर्शन कलेवर, उनकी शानदार प्रिटिंग और प्रस्तुति सारा कुछ बदला है। वे अब पढ़े जाने के साथ-साथ देखे जाने लायक भी बने हैं। किंतु क्या कारण है उनकी पठनीयता बहुत प्रभावित हो रही है। वे अब पढ़े जाने के बजाए पलटे ज्यादा जा रहे हैं। पाठक एक स्टेट्स सिंबल के चलते घरों में अखबार तो बुलाने लगा है, किंतु वह इन अखबारों पर वक्त नहीं दे रहा है। क्या कारण है कि ज्वलंत सवालों पर बौद्धिकता और विमर्शों का सारा काम अब अंग्रेजी अखबारों के भरोसे छोड़ दिया गया है? हिंदी अखबारों में अंग्रेजी के जो लेखक अनूदित होकर छप रहे हैं वह भी सेलिब्रेटीज ज्यादा हैं, बौद्धिक दुनिया के लोग कम । हिंदी की इतनी बड़ी दुनिया के पास आज भी ‘द हिंदू’ या ‘इंडियन एक्सप्रेस’ जैसा एक भी अखबार क्यों नहीं है, यह बात चिंता में डालने वाली है। कम पाठक, सीमित स्वीकार्यता के बजाए अंग्रेजी के अखबारों में हमारी कलाओं, किताबों, फिल्मों और शेष दुनिया की हलचलों पर बात करने का वक्त है तो हिंदी के अखबार इनसे मुंह क्यों चुरा रहे हैं।
हिंदी के एक बड़े लेखक अशोक वाजपेयी कह रहे हैं कि–
“पत्रकारिता में विचार अक्षमता बढ़ती जा रही है, जबकि उसमें यह स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। हिंदी में यह क्षरण हर स्तर पर देखा जा सकता है। हिंदी के अधिकांश अखबार और समाचार-पत्रिकाओं का भाषा बोध बहुत शिथिल और गैरजिम्मेदार हो चुका है। जो माध्यम अपनी भाषा की प्रामणिकता आदि के प्रति सजग नहीं हैं, उनमें गहरा विचार भी संभव नहीं है। हमारी अधिकांश पत्रकारिता, जिसकी व्याप्ति अभूतपूर्व हो चली है, यह बात भूल ही गयी है कि बिना साफ-सुथरी भाषा के साफ-सुथरा चिंतन भी संभव नहीं है।” (जनसत्ता,26 अप्रैल,2015)
श्री वाजपेयी का चिंताएं हिंदी समाज की साझा चिंताएं हैं। हिंदी के पाठकों, लेखकों, संपादकों और समाचारपत्र संचालकों को मिलकर अपनी भाषा और उसकी पत्रकारिता के सामने आ रहे संकटों पर बात करनी ही चाहिए। यह देखना रोचक है कि हिंदी की पत्रकारिता के सामने आर्थिक संकट उस तरह से नहीं हैं जैसा कि भाषायी या बौद्धिक संकट। हमारे समाचारपत्र अगर समाज में चल रही हलचलों, आंदोलनों और झंझावातों की अभिव्यक्ति करने में विफल हैं और वे बौद्धिक दुनिया में चल रहे विमर्शों का छींटा भी अपने पाठकों पर नहीं पड़ने दे रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि आखिर हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी अपने पाठकों का रूचि परिष्कार भी रही है। साथ ही हमारा काम अपने पाठक का उसकी भाषा और समाज के साथ एक रिश्ता बनाना भी है।
सूचना और मनोरंजन से आगे बढ़ना होगाः आखिर हमारे हिंदी अखबारों के पाठक को क्यों नहीं पता होना चाहिए कि उसके आसपास के परिवेश में क्या घट रहा है। हमारे पाठक के पास चीजों के होने और घटने की प्रक्रिया के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर विश्लेषण क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों वह गंभीर विमर्शों के लिए अंग्रेजी या अन्य भाषाओं पर निर्भर हो? हिंदी क्या सिर्फ सूचना और मनोरंजन की भाषा बनकर रह जाएगी? अपने बौद्धिक विश्लेषणों, सार्थक विमर्शों के आधार पर नहीं, सिर्फ चमकदार कागज पर शानदार प्रस्तुति के कारण ही कोई पत्रकारिता लोकस्वीकृति पा सकती है? आज का पाठक समझदार, जागरूक और विविध दूसरे माध्यमों से सूचना और विश्वेषण पाने की क्षमता से लैस है। ऐसे में हिंदी के अखबारों को यह सोचना होगा कि वे कब तक अपनी छाप-छपाई और प्रस्तुति के आधार पर लोगों की जरूरत बने रहेंगें।
गहरी सांस्कृतिक निरक्षरता से मुक्ति जरूरीः पठनीयता का संकट, सोशल मीडिया का बढ़ता असर, मीडिया के कंटेट में तेजी से आ रहे बदलाव, निजी नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता के सवाल, मोबाइल संस्कृति से उपजी चुनौतियों के बीच मूल्यों की बहस को देखा जाना चाहिए। इस समूचे परिवेश में आदर्श, मूल्य और सिद्धांतों की बातचीत भी बेमानी लगने लगी है। बावजूद इसके एक सुंदर दुनिया का सपना, एक बेहतर दुनिया का सपना देखने वाले लोग हमेशा एक स्वस्थ और सरोकारी मीडिया की बहस के साथ खड़े रहेंगे। संवेदना, मानवीयता और प्रकृति का साथ ही किसी भी संवाद माध्यम को सार्थक बनाता है। संवेदना और सरोकार समाज जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, तो मीडिया उससे अछूता कैसे रह सकता है। सही मायने में यह समय गहरी सांस्कृतिक निरक्षता और संवेदनहीनता का समय है। इसमें सबके बीच मीडिया भी गहरे असमंजस में है। लोक के साथ साहचर्य और समाज में कम होते संवाद ने उसे भ्रमित किया है। चमकती स्क्रीनों, रंगीन अखबारों और स्मार्ट हो चुके मोबाइल उसके मानस और कृतित्व को बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में मूल्यों की बात कई बार नक्कारखाने में तूती की तरह लगती है। किंतु जब मीडिया के विमर्शकार, संचालक यह सोचने बैठेंगे कि मीडिया किसके लिए और क्यों- तब उन्हें इसी समाज के पास आना होगा। रूचि परिष्कार, मत निर्माण की अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करना होगा। तभी मीडिया की सार्थकता है और तभी उसका मूल्य है । लाख मीडिया क्रांति के बाद भी ‘भरोसा’ वह शब्द है जो आसानी से अर्जित नहीं होता। लाखों का प्रसार आपके प्राणवान और सच के साथ होने की गारंटी नहीं है। ‘विचारों के अनुकूलन’ के समय में भी लोग सच को पकड़ लेते हैं। मीडिया का काम सूचनाओं का सत्यान्वेषण ही है, वरना वे सिर्फ सूचनाएं होंगी- खबर या समाचार नहीं बन पाएंगी।
इलेक्ट्रानिक मीडिया के नाते बढ़ा संकटः एक समय में प्रिंट मीडिया ही सूचनाओं का वाहक था, वही विचारों की जगह भी था। 1990 के बाद टीवी घर-घर पहुंचा और उदारीकरण के बाद निजी चैनलों की बाढ़ आ गयी। इसमें तमाम न्यूज चैनल भी आए। जल्दी सूचना देने की होड़ और टीआरपी की जंग ने माहौल को गंदला दिया। इसके बाद शुरू हुई टीवी बहसों ने तो हद ही कर दी। टीवी पर भाषा की भ्रष्टता, विवादों को बढ़ाने और अंतहीन बहसों की एक ऐसी दुनिया बनी जिसने टीवी स्क्रीन को चीख-चिल्लाहटों और शोरगुल से भर दिया। इसने हमारे एंकर्स, पत्रकारों और विशेषज्ञों को भी जगहंसाई का पात्र बना दिया। उनकी अनावश्यक पक्षधरता भी लोगों से सामने उजागर हुयी। ऐसे में भरोसा टूटना ही था। इसमें पाठक और दर्शक भी बंट गए। हालात यह हैं कि दलों के हिसाब से विशेषज्ञ हैं जो दलों के चैनल भी हैं। पक्षधरता का ऐसा नग्न तांडव कभी देखा नहीं गया। आज हालात यह हैं कि टीवी म्यूट (शांत) रखकर भी अनेक विशेषज्ञों के बारे में यह बताया जा सकता है कि वे क्या बोल रहे होंगे। इस समय का संकट यह है कि पत्रकार या विशेषज्ञ तथ्यपरक विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अपनी पक्षधरता को पूरी नग्नता के साथ व्यक्त करने में लगे हैं। ऐसे में सत्य और तथ्य सहमे खड़े रह जाते हैं। दर्शक अवाक रह जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। कहने में संकोच नहीं है कि अनेक पत्रकार, संपादक और विषय विशेषज्ञ दल विशेष के प्रवक्ताओं को मात देते हुए दिखते हैं। ऐसे में इस पूरी बौद्धिक जमात को वही आदर मिलेगा जो आप किसी दल के प्रवक्ता को देते हैं। मीडिया की विश्वसनीयता को नष्ट करने में टीवी मीडिया के इस ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित जरूर किया जाएगा। यह साधारण नहीं है कि टीवी के नामी एंकर भी अब टीवी न देखने की सलाहें दे रहे हैं। ऐसे में यह टीवी मीडिया कहां ले जाएगा कहना कठिन है।
सत्यान्वेषण से ही सार्थकताः कोई भी मीडिया सत्यान्वेषण की अपनी भूख से ही सार्थक बनता है, लोक में आदर का पात्र बनता है। हमें अपने मीडिया को मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों के साथ खड़ा करना होगा। यह शब्द आज की दुनिया में बोझ भले लगते हों पर किसी भी संवाद माध्यम को सार्थकता देने वाले शब्द यही हैं। सच की खोज कठिन है पर रुकी नहीं है। सच से साथ खड़े रहना कभी आसान नहीं था। हर समय अपने नायक खोज ही लेता है। इस कठिन समय में भी कुछ चमकते चेहरे हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे मूल्यों के साथ, आदर्शों की दिखाई राह पर अपने सिद्धांतों के साथ डटे हैं। समय ऐसे ही नायकों को इतिहास में दर्ज करता है और उन्हें ही मान देता है। हर समय अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर सामने आता है, उन सवालों से जूझकर ही नायक अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। नए समय ने अनेक संकट खड़े किए हैं तो अपार अवसर भी दिए भी हैं। भरोसे का बचाना जरुरी है, क्योंकि यही हमारी ताकत है। भरोसे का नाम ही पत्रकारिता है, सभी तंत्रों से निराश लोग अगर आज भी मीडिया की तरफ आस से देख रहे हैं तो तय मानिए मीडिया और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक ही हैं। गहरी लोकतांत्रिकता में रचा-बसा समाज ही एक अच्छे मीडिया का भी पात्र होता है। हमें अपने मनों में झांकना होगा कि क्या हमारी सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां एक बेहतर मीडिया के लिए, एक अच्छे मनुष्य के लिए उपयुक्त हैं? अगर नहीं तो मनुष्य की मुक्ति के अभी कुछ और जतन करने होंगे। लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र में बदलने के लिए और काम करना होगा। ऐसी सारी यात्राएं पत्रकारिता, कलाओं, साहित्य और सृजन की दुनिया को ज्यादा लोकतांत्रिक, ज्यादा विचारवान, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा मानवीय बनाएंगी। यह सृजनात्मक दुनिया एक बेहतर दुनिया को जल्दी संभव करेगी।
इ




